
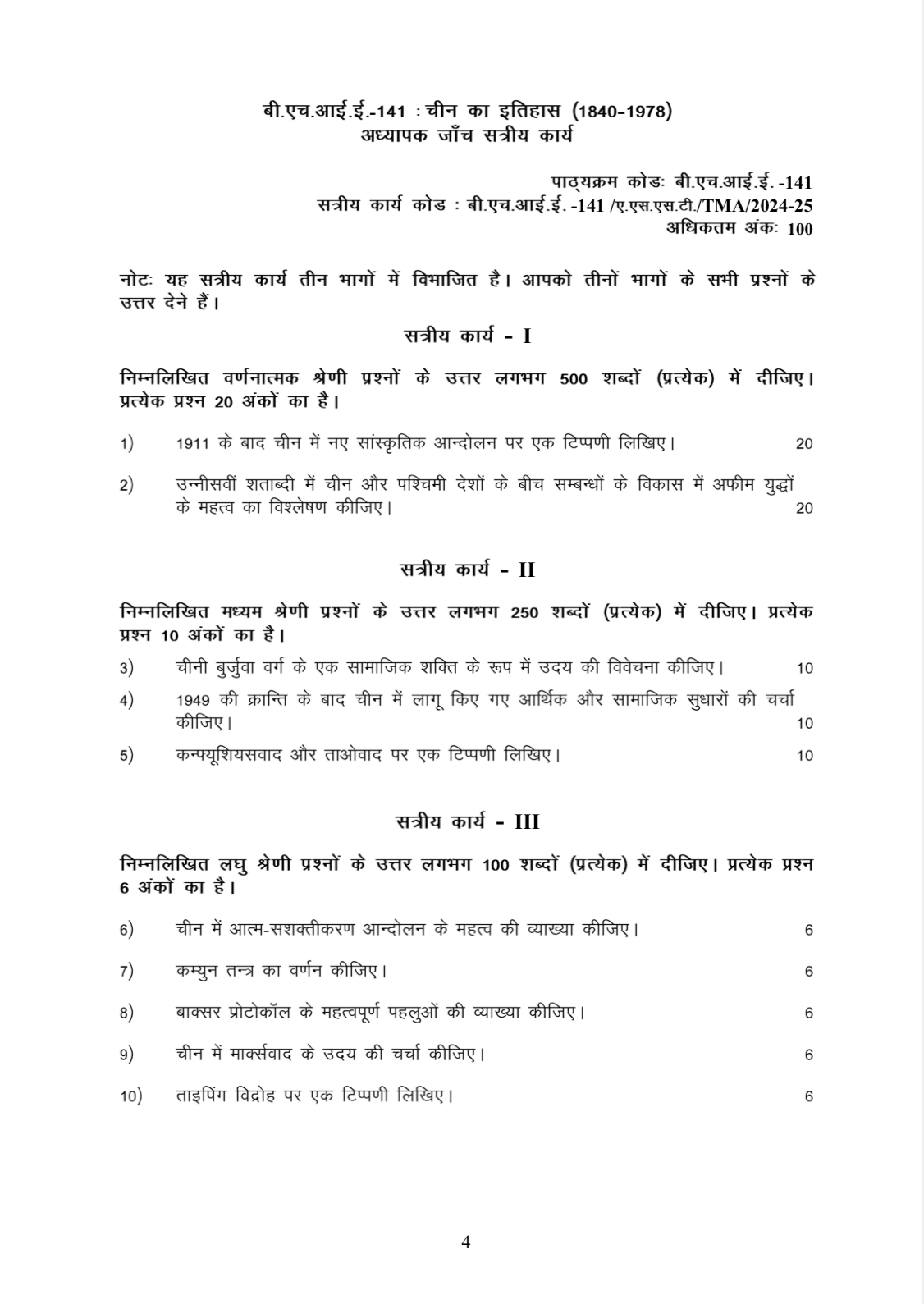
सत्रीय कार्य-I1) 1911 के बाद चीन में नए सांस्कृतिक आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए।उत्तर: 1911 की सिन्हाई क्रांति के बाद चीन में साम्राज्यवाद का अंत हुआ और चिंग वंश का पतन हो गया। इसके परिणामस्वरूप चीन गणराज्य की स्थापना हुई, लेकिन यह राजनीतिक परिवर्तन अपने साथ सामाजिक और सांस्कृतिक अस्थिरता भी लेकर आया। पारंपरिक मान्यताओं, विशेष रूप से कन्फ्यूशियसवाद, पर सवाल उठाए जाने लगे। इसी पृष्ठभूमि में नया सांस्कृतिक आंदोलन (New Culture Movement) का उदय हुआ, जो 1915 से 1925 के बीच चीनी समाज में व्यापक बौद्धिक और सांस्कृतिक बदलाव का प्रतीक बना।आंदोलन की पृष्ठभूमि1911 की क्रांति के बावजूद चीन में राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। पारंपरिक सामंती व्यवस्था और विदेशी हस्तक्षेप से प्रभावित समाज में आधुनिकता की मांग बढ़ी। इस दौरान कई बुद्धिजीवियों ने चीनी समाज को पश्चिमी आधुनिकता, विज्ञान और लोकतंत्र की ओर मोड़ने की कोशिश की। प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918) और 1919 के मई चौथा आंदोलन (May Fourth Movement) ने इस सांस्कृतिक पुनर्जागरण को और गति दी।आंदोलन के प्रमुख विचार और उद्देश्य1. परंपरावाद का विरोध – आंदोलन ने विशेष रूप से कन्फ्यूशियसवाद के कठोर नैतिक सिद्धांतों और पारंपरिक सामाजिक संरचना को चुनौती दी।2. लोकतंत्र और विज्ञान – बुद्धिजीवियों ने “लोकतंत्र (Democracy)” और “विज्ञान (Science)” को चीन के विकास के प्रमुख आधार के रूप में प्रचारित किया।3. भाषा सुधार – पारंपरिक क्लासिकल चीनी भाषा (वेन्येन) की जगह आम बोलचाल की भाषा (बाईहुआ) को अपनाने पर जोर दिया गया, ताकि शिक्षा और ज्ञान आम लोगों तक पहुंच सके।4. पश्चिमी विचारों का प्रसार – आंदोलन में पश्चिमी दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और लेखकों के कार्यों का अनुवाद किया गया। जॉन डेवी और बर्ट्रेंड रसेल जैसे पश्चिमी विचारकों के सिद्धांत चीन में लोकप्रिय हुए।5. महिला मुक्ति – आंदोलन के दौरान महिलाओं के अधिकारों और उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया, जिससे पारंपरिक पितृसत्तात्मक समाज में बदलाव आया।प्रमुख नेता और योगदान• चेन दुशिउ – उन्होंने “न्यू यूथ” पत्रिका के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किया और लोकतंत्र तथा विज्ञान को बढ़ावा दिया।• हू शि – उन्होंने भाषा सुधार का समर्थन किया और आम बोलचाल की भाषा को लेखन और शिक्षा में लागू करने की वकालत की।• लू शुन – उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से चीनी समाज की रूढ़िवादिता की आलोचना की, विशेष रूप से उनकी कहानी “क्यूआनजी की डायरी” बहुत प्रसिद्ध हुई।मई चौथा आंदोलन और प्रभाव1919 में वर्साय संधि के विरोध में चीन में मई चौथा आंदोलन हुआ, जिसमें छात्रों, बुद्धिजीवियों और श्रमिकों ने राष्ट्रवादी आंदोलन को समर्थन दिया। इस आंदोलन ने नया सांस्कृतिक आंदोलन को एक नई दिशा दी और राष्ट्रीय पुनरुत्थान की भावना को मजबूत किया।निष्कर्षनया सांस्कृतिक आंदोलन चीन में आधुनिकता और प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास था। इसने परंपरागत रूढ़ियों को चुनौती दी, भाषा और शिक्षा में सुधार किए, तथा लोकतंत्र और विज्ञान को अपनाने का मार्ग प्रशस्त किया। यह आंदोलन आगे चलकर चीन में साम्यवादी विचारधारा के उदय और 1949 की क्रांति का भी आधार बना। इस प्रकार, यह आधुनिक चीन के निर्माण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था।2) उन्नीसवीं शताब्दी में चीन और पश्चिमी देशों के बीच संबंधों के विकास में अफीम युद्धों के महत्व का विश्लेषण कीजिए।उत्तर: उन्नीसवीं शताब्दी में चीन और पश्चिमी देशों के बीच संबंधों के विकास में अफीम युद्धों का महत्व
उन्नीसवीं शताब्दी में चीन और पश्चिमी देशों के बीच संबंधों के विकास में अफीम युद्धों (1839-42 और 1856-60) की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये युद्ध केवल व्यापारिक संघर्ष नहीं थे, बल्कि उन्होंने चीन के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को गहराई से प्रभावित किया। इन युद्धों के परिणामस्वरूप चीन की पारंपरिक व्यवस्था कमजोर हुई और पश्चिमी प्रभाव बढ़ता गया।
अफीम व्यापार और युद्ध का कारण
अठारहवीं शताब्दी के अंत तक, ब्रिटेन चीन से चाय, रेशम और चीनी जैसी वस्तुएँ बड़ी मात्रा में खरीद रहा था, लेकिन बदले में चीन ब्रिटेन से बहुत कम सामान खरीदता था। इस व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए ब्रिटिश व्यापारियों ने चीन में अफीम बेचना शुरू किया, जिसे भारत में उगाया जाता था।
चीन में अफीम की लत तेजी से बढ़ने लगी, जिससे समाज में गंभीर सामाजिक और आर्थिक समस्याएँ उत्पन्न हुईं। चीन की किंग सरकार ने इस समस्या को रोकने के लिए 1839 में अफीम व्यापार पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया और अफीम के भंडार नष्ट कर दिए। इस कदम से ब्रिटेन नाराज हुआ और उसने चीन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, जिसे पहला अफीम युद्ध (1839-42) कहा जाता है।
पहला और दूसरा अफीम युद्ध: परिणाम और प्रभाव
पहले अफीम युद्ध में चीन की हार हुई और 1842 में उसे नानकिंग संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। इस संधि के तहत:
1. हांगकांग को ब्रिटेन को सौंप दिया गया।
2. पाँच चीनी बंदरगाह—ग्वांगझोउ, शंघाई, फुज़ोउ, निंगबो और जिआमेन—पश्चिमी व्यापार के लिए खोल दिए गए।
3. चीन को ब्रिटेन को बड़ी क्षतिपूर्ति देनी पड़ी।
लेकिन यह संधि ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी देशों को संतुष्ट नहीं कर सकी। 1856 में ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर दूसरा अफीम युद्ध छेड़ दिया। 1860 में बीजिंग संधि के तहत:
1. चीन ने और अधिक बंदरगाह विदेशी व्यापार के लिए खोल दिए।
2. विदेशी व्यापारियों और ईसाई मिशनरियों को पूरे चीन में स्वतंत्र रूप से आने-जाने की अनुमति मिली।
3. चीन को और अधिक धनराशि का भुगतान करना पड़ा।
अफीम युद्धों का दीर्घकालिक प्रभाव
1. चीन की संप्रभुता का ह्रास: इन युद्धों ने चीन की परंपरागत राजनीतिक शक्ति को कमजोर कर दिया और उसे पश्चिमी देशों के अधीन कर दिया।
2. अन्यायपूर्ण संधियाँ: चीन को बार-बार अपमानजनक संधियों पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिन्हें “अन्यायपूर्ण संधियाँ” कहा गया।
3. पश्चिमी प्रभाव का बढ़ना: अफीम युद्धों के बाद चीन में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और अमेरिका का प्रभाव बढ़ गया।
4. आर्थिक और सामाजिक संकट: अफीम की लत और युद्धों की क्षति ने चीनी समाज में असंतोष बढ़ाया, जिससे ताइपिंग विद्रोह (1850-64) और बाद में बॉक्सर विद्रोह (1899-1901) जैसे आंदोलनों को बढ़ावा मिला।
5. आधुनिकीकरण की प्रक्रिया: इन पराजयों से सबक लेते हुए चीन ने अपनी सैन्य और औद्योगिक क्षमता को बढ़ाने के लिए “आत्म-सुदृढ़ीकरण आंदोलन” (Self-Strengthening Movement) की शुरुआत की।
निष्कर्ष
अफीम युद्धों ने चीन और पश्चिमी देशों के संबंधों को एक निर्णायक मोड़ दिया। चीन, जो पहले खुद को दुनिया का केंद्र मानता था, पश्चिमी शक्तियों के दबाव में आ गया। ये युद्ध चीन के “अर्ध-उपनिवेशीकरण” की शुरुआत थे और उन्होंने चीन की राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया। इसके परिणामस्वरूप चीन में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जिसने बीसवीं शताब्दी में साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष को जन्म दिया।
सत्रीय कार्य-II
3) चीनी बुर्जुवा वर्ग के एक सामाजिक शक्ति के रूप में उदय की विवेचना कीजिए।
उत्तर: चीनी बुर्जुआ वर्ग के एक सामाजिक शक्ति के रूप में उदयचीन में बुर्जुआ वर्ग (बौर्ज़्वा वर्ग) का उदय एक जटिल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रिया का परिणाम है, जिसे मुख्य रूप से आर्थिक सुधारों और वैश्वीकरण ने बढ़ावा दिया। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, विशेष रूप से 1978 के बाद, देंग शियाओपिंग द्वारा शुरू किए गए आर्थिक उदारीकरण और “सुधार एवं खुलापन” (Reform and Opening-up) नीति के तहत निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया। इससे एक नए मध्यम वर्ग और बुर्जुआ वर्ग का निर्माण हुआ, जिसने चीनी समाज में एक प्रभावशाली सामाजिक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाई।चीनी बुर्जुआ वर्ग मुख्य रूप से निजी उद्यमियों, व्यापारियों, पेशेवरों और उच्च वेतनभोगी कर्मचारियों से मिलकर बना है। 1990 और 2000 के दशक में चीन की तीव्र आर्थिक वृद्धि ने इस वर्ग को सशक्त बनाया। वैश्विक व्यापार और निवेश में चीन की बढ़ती भागीदारी ने निजी कंपनियों को फलने-फूलने का अवसर दिया, जिससे संपत्ति, आय और जीवनशैली में भारी बदलाव आया।सामाजिक दृष्टिकोण से, यह वर्ग उपभोक्तावाद, शहरीकरण और आधुनिक जीवनशैली को बढ़ावा देता है। इसने चीन में शिक्षा, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक परिवर्तनों को गति दी है। राजनीतिक रूप से, हालांकि चीन में एक-पार्टी शासन (चीनी कम्युनिस्ट पार्टी) कायम है, लेकिन बुर्जुआ वर्ग नीतिगत मामलों और आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने लगा है।हालांकि, चीनी बुर्जुआ वर्ग को सरकारी नियंत्रण, आय असमानता और सामाजिक अस्थिरता जैसी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। फिर भी, यह वर्ग आधुनिक चीन के विकास और वैश्विक शक्ति के रूप में उसके उभरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।4) 1949 की क्रांति के बाद चीन में लागू किए गए आर्थिक और सामाजिक सुधारों की चर्चा कीजिए।उत्तर: 1949 की क्रांति के बाद चीन में लागू किए गए आर्थिक और सामाजिक सुधार1949 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) के नेतृत्व में माओ ज़ेदोंग ने क्रांति के माध्यम से चीन में साम्यवादी शासन स्थापित किया। इसके बाद चीन ने कई महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक सुधार लागू किए, जिनका उद्देश्य देश को आत्मनिर्भर, औद्योगिक और समाजवादी राष्ट्र बनाना था।
आर्थिक सुधार
- भूमि सुधार (1950-1952): जमींदारी प्रथा समाप्त की गई और गरीब किसानों में भूमि का पुनर्वितरण किया गया।
- पहला पंचवर्षीय योजना (1953-1957): सोवियत संघ की मदद से चीन में भारी उद्योगों का विकास किया गया।
- महान उछाल (1958-1962): कृषि और औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए सामूहिक खेती (कम्यून सिस्टम) लागू की गई, लेकिन यह नीति असफल रही और बड़े पैमाने पर अकाल पड़ा।
- सुधार और खुलेपन की नीति (1978): देंग शियाओपिंग के नेतृत्व में चीन ने आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई, जिससे निजी उद्यमों को बढ़ावा मिला और वैश्विक व्यापार में चीन की भागीदारी बढ़ी।
सामाजिक सुधार
- शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार: साक्षरता दर बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाओं को गाँवों तक पहुँचाने के लिए प्रयास किए गए।
- सांस्कृतिक क्रांति (1966-1976): माओ ने विचारधारात्मक सुधारों के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की, लेकिन इससे समाज में अस्थिरता बढ़ी।
- एक-बच्चा नीति (1980): जनसंख्या नियंत्रण के लिए इसे लागू किया गया।
इन सुधारों से चीन ने तेज़ी से आर्थिक प्रगति की और 21वीं सदी में वैश्विक महाशक्ति बनकर उभरा।
5) कन्फ्यूशियसवाद और ताओवाद पर एक टिपण्णी लिखिए।उत्तर: कन्फ्यूशियसवाद और ताओवाद प्राचीन चीन के दो प्रमुख दार्शनिक एवं नैतिक विचारधाराएं हैं, जो चीनी समाज, संस्कृति और राजनीति को गहराई से प्रभावित करती रही हैं।कन्फ्यूशियसवाद की स्थापना महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस (551-479 ईसा पूर्व) ने की थी। यह विचारधारा नैतिकता, सामाजिक व्यवस्था और अनुशासन पर केंद्रित है। कन्फ्यूशियस ने पारिवारिक मूल्यों, शिक्षा, परंपराओं और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दिया। उनके अनुसार, व्यक्ति को "रिन" (करुणा), "ली" (शिष्टाचार) और "शाओ" (बड़ों के प्रति सम्मान) का पालन करना चाहिए। कन्फ्यूशियसवाद ने चीन में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया और सदियों तक सरकारी नौकरियों में इसका प्रभाव बना रहा।ताओवाद की स्थापना लाओत्ज़ु (6वीं शताब्दी ईसा पूर्व) ने की थी। यह विचारधारा प्रकृति के साथ सामंजस्य, सरलता और सहजता को महत्व देती है। ताओवाद "ताओ" (मार्ग या प्रकृति का नियम) के सिद्धांत पर आधारित है, जो सिखाता है कि व्यक्ति को प्रकृति के प्रवाह के साथ चलना चाहिए और अनावश्यक संघर्ष से बचना चाहिए। "वू वेई" (कर्म में अकर्म) ताओवाद का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि अत्यधिक हस्तक्षेप के बजाय प्राकृतिक रूप से कार्य करना चाहिए। ताओवाद का प्रभाव चिकित्सा, कला और मार्शल आर्ट्स में भी देखा जाता है।कन्फ्यूशियसवाद समाज और नैतिक कर्तव्यों को प्राथमिकता देता है, जबकि ताओवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रकृति के साथ सामंजस्य पर बल देता है। दोनों विचारधाराओं ने चीनी संस्कृति और जीवनशैली को गहराई से प्रभावित किया है और आज भी इनका प्रभाव देखा जा सकता है।सत्रीय कार्य-III6) चीन में आत्म शक्तिकरण आंदोलन के महत्व की व्याख्या
कीजिए।
उत्तर: चीन में आत्म शक्तिकरण आंदोलन (Self-Strengthening Movement) 1861 से 1895 तक चला, जिसका उद्देश्य चीन को बाहरी आक्रमणों और आंतरिक कमजोरी से बचाने के लिए सैन्य और औद्योगिक सुधार लाना था। यह आंदोलन पश्चिमी तकनीक और विज्ञान अपनाकर चीन की रक्षा और आर्थिक शक्ति बढ़ाने पर केंद्रित था। हालांकि, यह पारंपरिक कन्फ्यूशियस विचारधारा से प्रभावित था, जिससे इसमें राजनीतिक और सामाजिक सुधार सीमित रहे। आंदोलन के अंतर्गत आधुनिक शस्त्रागार, नौसेना और संचार सुविधाओं का विकास हुआ, लेकिन सरकारी भ्रष्टाचार और असंगठित नीतियों के कारण यह पूरी तरह सफल नहीं हो सका, जिससे अंततः चीन पर विदेशी प्रभुत्व बढ़ता गया।7) कम्युन तंत्र का वर्णन कीजिए।उत्तर: कम्युन तंत्र का वर्णनकम्युन तंत्र एक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है जिसमें संसाधनों और उत्पादन के साधनों का सामूहिक स्वामित्व होता है। इसमें निजी संपत्ति के स्थान पर सामूहिक संपत्ति को महत्व दिया जाता है, और समाज के सभी लोग समान रूप से संसाधनों का उपयोग करते हैं।चीन में "महान अग्रगामी छलांग" (1958-1962) के दौरान कम्युन तंत्र को अपनाया गया, जहां कृषि और उद्योग का सामूहिकरण किया गया। गांवों में जन कम्यून बनाए गए, जहां लोग सामूहिक रूप से काम और जीवन व्यतीत करते थे। हालांकि, कुप्रबंधन और प्राकृतिक आपदाओं के कारण यह तंत्र विफल हो गया।कम्युन तंत्र का उद्देश्य समानता और सामूहिक भागीदारी को बढ़ावा देना था, लेकिन इसकी कठोर नीतियों से कई आर्थिक और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुईं।8) बाक्सर प्रोटोकॉल के महत्वपूर्ण पहलुओं की व्याख्या कीजिए।उत्तर: बाक्सर प्रोटोकॉल (Boxer Protocol) के महत्वपूर्ण पहलूबाक्सर प्रोटोकॉल 7 सितंबर 1901 को चीन और 11 विदेशी शक्तियों के बीच हस्ताक्षरित एक संधि थी, जो 1899-1901 के बाक्सर विद्रोह के बाद हुई। इसके प्रमुख पहलू निम्नलिखित थे:
- हर्जाना: चीन को 450 मिलियन टेल (चांदी) का मुआवजा देना पड़ा।
- विदेशी सेना की तैनाती: बीजिंग और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में विदेशी सैनिकों की स्थायी उपस्थिति सुनिश्चित की गई।
- किलेबंदी निषेध: चीन को कई किलों को नष्ट करना पड़ा।
- विदेशी नागरिकों की सुरक्षा: चीन को राजनयिकों और मिशनरियों की सुरक्षा की गारंटी देनी पड़ी।
- चीन की संप्रभुता पर प्रभाव: इस संधि ने चीन की राष्ट्रीय संप्रभुता को कमजोर किया और पश्चिमी शक्तियों का प्रभाव बढ़ाया।
9) चीन में मार्क्सवाद के उदय की चर्चा कीजिए।उत्तर: चीन में मार्क्सवाद का उदयचीन में मार्क्सवाद का उदय 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ, जब 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरित होकर कई चीनी बुद्धिजीवी और नेता समाजवाद की ओर आकर्षित हुए। मई चौथी आंदोलन (1919) ने साम्राज्यवाद और पारंपरिक विचारों के खिलाफ संघर्ष को तेज किया, जिससे मार्क्सवादी विचारों का प्रसार हुआ।1921 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) की स्थापना हुई, जिसने मार्क्सवाद-लेनिनवाद को अपनाया। माओत्से तुंग के नेतृत्व में यह विचारधारा ग्रामीण किसानों के समर्थन के साथ आगे बढ़ी और 1949 में कम्युनिस्ट क्रांति के बाद चीन की आधिकारिक विचारधारा बन गई। मार्क्सवाद ने चीन की सामाजिक और आर्थिक नीतियों को गहराई से प्रभावित किया।10) ताइपिंग विद्रोह पर एक टिप्पणी लिखिए।उत्तर: ताइपिंग विद्रोह: एक टिप्पणीताइपिंग विद्रोह (1850-1864) चीन के इतिहास का सबसे बड़ा जनविद्रोह था, जिसका नेतृत्व होंग शिउछान ने किया। उन्होंने स्वयं को मसीहा घोषित किया और "ताइपिंग स्वर्गीय राज्य" की स्थापना का दावा किया।विद्रोह का मुख्य कारण किंग वंश की भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता और विदेशी प्रभाव था। ताइपिंग सेना ने नानजिंग पर कब्जा कर उसे अपनी राजधानी बनाया। हालांकि, किंग शासन ने ब्रिटेन और फ्रांस की मदद से विद्रोह को कुचल दिया।इस विद्रोह में लगभग दो करोड़ लोग मारे गए, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था और समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। यह विद्रोह आगे चलकर चीन में सुधारवादी आंदोलनों की प्रेरणा बना।
Mulsif Publication
Website:- https://www.mulsifpublication.in
Contact:- tsfuml1202@gmail.com
No comments:
Post a Comment